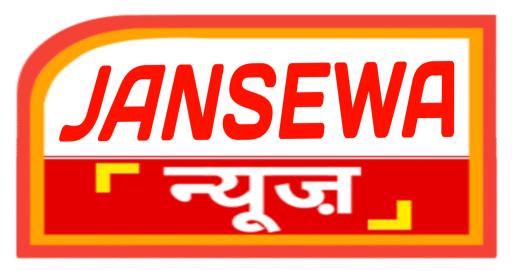नई दिल्ली: राज्यपालों को राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों पर अनिश्चित काल तक बैठने की अनुमति देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोगों की वसीयत को “दोषपूर्ण” कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देखा, क्योंकि इसने राष्ट्रपति के संदर्भ को सुनकर जारी रखा कि क्या अदालतें गुबरैनी और राष्ट्रपति पद के लिए समयसीमा लिख सकती हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) भूषण आर गवई और जस्टिस सूर्य कांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिम्हा और अतुल एस चंदूरकर की एक संविधान बेंच मई में किए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुरमू के अनुच्छेद 143 संदर्भ की जांच कर रही है। संदर्भ शीर्ष अदालत के 8 अप्रैल के फैसले पर स्पष्टता चाहता है, जिसने पहली बार राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित की, जो उनके सामने लंबित राज्य बिलों पर निर्णय लेने के लिए।
“यदि कोई विशेष कार्य राज्यपाल को सौंपा जाता है और वर्षों तक वह इसे वापस ले लेता है, तो क्या यह भी इस न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के दायरे से परे होगा? जब इस अदालत ने मूल संरचना का उल्लंघन करने के रूप में न्यायिक समीक्षा को दूर करने के लिए संवैधानिक संशोधनों को अलग कर दिया है, तो क्या अब हम यह कह सकते हैं कि उच्च संवैधानिक प्राधिकारी हो सकता है, अदालतें अभी भी शक्तिहीन हो जाएंगी यदि यह कार्य नहीं करता है?” बेंच ने पूछा।
बेंच ने यह भी बताने के लिए केंद्र को दबाया कि जब राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए कार्रवाई में देरी करते हैं तो क्या उपाय मौजूद है। “अनुच्छेद 200 के तहत, अगर हम यह मानते हैं कि राज्यपाल के पास समय के लिए एक बिल को वापस लेने की असीमित शक्ति है, तो एक विधिवत निर्वाचित विधायिका के लिए सुरक्षा क्या है? मान लीजिए कि दो-तिहाई बहुमत द्वारा चुने गए विधानमंडल ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है, और गवर्नर बस इस पर बैठता है, यह विधानमंडल को पूरी तरह से खराब कर देगा।”
सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने केंद्र सरकार के लिए उपस्थित होते हुए कहा कि अदालत की चिंता को उचित ठहराया जा सकता है, यह समय सीमा निर्धारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं मान सकता है जहां संविधान चुप है। “एक औचित्य कभी भी अधिकार क्षेत्र को प्रदान नहीं कर सकता है। इस देश की हर समस्या का सर्वोच्च न्यायालय में कोई समाधान नहीं हो सकता है। कुछ समस्याओं को सिस्टम के भीतर समाधान खोजना होगा,” उन्होंने कहा।
मेहता के अनुसार, समाधान “राजनीतिक प्रक्रिया में, न्यायिक निर्देश नहीं” में था। उन्होंने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री इस तरह के आवेगों को हल करने के लिए सीधे राज्यपालों, प्रधानमंत्रियों या राष्ट्रपति के साथ जुड़ सकते हैं।
“इस तरह के मुद्दे दशकों से उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन हमेशा राजनीतिक राज्यों और परिपक्वता के माध्यम से हल किया गया है। हम अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? उपाय अंततः एक संशोधन के माध्यम से संसद के साथ झूठ बोलेंगे, न्यायिक कानून द्वारा नहीं,” मेहता ने प्रस्तुत किया।
इस पर, बेंच ने हस्तक्षेप किया: “जब कोई बाहरी सीमा नहीं होती है, तो क्या एक संवैधानिक व्याख्या को एक वैक्यूम के लिए छोड़ दिया जा सकता है? हालांकि एक समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, किसी भी तरह से प्रक्रिया काम करती है। ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है जहां एक बिल पर काम नहीं करना एक पूर्ण विराम है … आगे कुछ भी नहीं।”
पीठ ने यह भी सवाल किया कि क्या न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से बाहर रखा जा सकता है। अदालत ने देखा: “निर्णय न्यायसंगत नहीं हो सकता है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है।”
हालांकि, मेहता ने चेतावनी दी कि जांच के लिए दरवाजा खोलने से गवर्नर या राष्ट्रपति के फैसले के हर चरण में लेख 200 और 201 के तहत “बहुस्तरीय चुनौतियां” हो जाएंगी। “अंतिम निर्णय से पहले हमारी समस्या हर कदम है, क्योंकि वे भी एक ‘निर्णय’ का गठन कर सकते हैं,” उन्होंने तर्क दिया। उन्होंने न्यायिक मिसालों का हवाला दिया, जहां अदालत ने कहा कि आपराधिक परीक्षणों के लिए निश्चित समयसीमा न्यायिक रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती है, उनके प्रस्तुत करने को सुदृढ़ करने के लिए कि संवैधानिक प्रक्रियाओं में समयसीमा भी न्यायिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।
लेकिन बेंच ने केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल द्वारा पहले से ही दायर याचिकाओं का हवाला देते हुए आगे दबाया। “मान लीजिए कि एक निर्णय चार साल के लिए नहीं लिया गया है। सरकार के लोकतांत्रिक सेट-अप का क्या होता है? विधायिका के दो-तिहाई बहुमत की इच्छा का क्या होता है?” यह पूछा।
मेहता ने एक सादृश्य के साथ जवाब दिया: “10 वर्षों के लिए लंबित परीक्षण का उदाहरण लें। क्या राष्ट्रपति कदम रख सकते हैं और घोषणा कर सकते हैं कि सजा को समझा जाता है क्योंकि न्यायपालिका में देरी हुई है? शक्तियों के पृथक्करण का मतलब है कि कुछ मुद्दे गैर-न्यायसंगत हैं।”
अदालत ने, हालांकि, यह स्पष्ट किया कि यह एक काल्पनिक चिंता से नहीं निपट रहा था। “हम कम से कम चार राज्यों से याचिकाएं कर रहे हैं,” अदालत ने रेखांकित किया।
तमिलनाडु मामले में अदालत के अप्रैल के फैसले से प्रेरित राष्ट्रपति संदर्भ, पूछता है कि क्या न्यायपालिका गवर्नर और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक अधिकारियों पर समयसीमा लगा सकती है जब संविधान स्वयं चुप है। उस फैसले में, एक दो-न्यायाधीश की पीठ ने भी राष्ट्रपति के लिए एक राज्यपाल द्वारा संदर्भित बिलों पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की, और एक महीने में एक राज्यपाल के लिए फिर से लागू किए गए बिलों पर कार्य करने के लिए। यहां तक कि इसने 10 तमिलनाडु बिलों को स्वीकार करने के लिए अनुच्छेद 142 को भी लागू किया था, यह मानने के बाद कि गवर्नर की लंबी निष्क्रियता “अवैध” थी।
मेहता ने डीम्ड असेंट की धारणा की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया, “समझा गया कि आपके लॉर्डशिप ने गवर्नर के लिए अपने आप को प्रतिस्थापित किया और स्वीकृति को घोषित कर दिया।
हालांकि, पीठ ने कहा कि अदालतें संविधान के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को समाप्त नहीं कर सकती हैं। “हर गलत के पास एक उपाय होना चाहिए। क्या संवैधानिक न्यायालय के हाथ तब बंधे होंगे जब एक संवैधानिक कार्यकर्ता बिना किसी वैध कारण के अपने कार्य का निर्वहन करने से इनकार करता है? क्या अदालत कहेगी कि हम शक्तिहीन हैं?” बेंच ने पूछा।
संदर्भ पर तर्क 26 अगस्त को जारी रहेगा।